मुहम्मद इक़बाल
मुहम्मद इक़बाल (उर्दू: محمد اقبال) (जीवन: 9 नवम्बर 1877 – 21 अप्रैल 1938) अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फ़ारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है।
इकबाल के दादा सहज सप्रू हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सिआलकोट आ गए।[1]
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: असरार-ए-ख़ुदी, रुमुज़-ए-बेख़ुदी और बंग-ए-दारा, जिसमें देशभक्तिपूर्ण तराना-ए-हिन्द (सारे जहाँ से अच्छा) शामिल है। फ़ारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ इन्हें इक़बाल-ए-लाहौर कहा जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनैतिक दर्शन पर काफ़ी लिखा है।
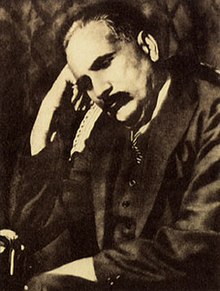 | |
| व्यक्तिगत जानकारी | |
|---|---|
| अन्य नाम | अल्लमा इक़बाल |
| जन्म | 9 नवम्बर 1877 सियालकोट, पंजाब, ब्रितानी भारत |
| मृत्यु | 21 अप्रैल 1938 (उम्र 60 वर्ष) लाहौर, पंजाब, भारत |
| वृत्तिक जानकारी | |
| युग | २०वीं सदी के दार्शनिक |
| क्षेत्र | ब्रितानी भारत |
| मुख्य विचार | शायरी, फ़ारसी कवितायें |
| प्रमुख विचार | दो-क़ौमी नज़रिया, पाकिस्तान की अवधारणा |
प्रभावित
मोहम्मद अली जिन्ना, इस्लामी जम्हूरिया-ए-पाकिस्तान
| |
| वेबसाइट | अल्लमा इक़बाल |
तराना-ए-मिल्ली (उर्दू: ترانۂ ملی) या समुदाय का गान एक उत्साही कविता है जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम उम्माह (इस्लामिक राष्ट्रों) को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस्लाम में राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने दुनिया में कहीं भी रह रहे सभी मुसलमानों को एक ही राष्ट्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी, जिसके नेता मुहम्मद हैं, जो मुसलमानों के पैगंबर है।
इक़बाल ने हिन्दोस्तान की आज़ादी से पहले "तराना-ए-हिन्द" लिखा था, जिसके प्रारंभिक बोल- "सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा" कुछ इस तरह से थे। उस समय वो इस सामूहिक देशभक्ति गीत से अविभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक रहने की नसीहत देते थे और और वो इस गीत के कुछ अंश में सभी धर्मों के लोगों को 'हिंदी है हम वतन है' कहकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की प्रेरणा देते है।
उन्होंने पाकिस्तान के लिए "तराना-ए-मिली" (मुस्लिम समुदाय के लिए गीत) लिखा, जिसके बोल- "चीन-ओ-अरब हमारा, हिन्दोस्तां हमारा ; मुस्लिम है वतन है, सारा जहाँ हमारा..."
कुछ इस तरह से है। यह उनके 'मुस्लिम लीग' और "पाकिस्तान आंदोलन" समर्थन को दर्शाता है।
इकबाल पाकिस्तान का जनक बन गए क्योंकि वह "पंजाब, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाने की अपील करने वाले पहले व्यक्ति थे", इंडियन मुस्लिम लीग के २१ वें सत्र में ,उनके अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था जो २९ दिसंबर,१९३० को इलाहाबाद में आयोजित की गई थी।[2] भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इक़बाल ने ही उठाया था[3][4]। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की माँग उठाई[5]। इसके बाद इन्होंने जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनके साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया[6]। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रकवि माना जाता है। इन्हें अलामा इक़बाल (विद्वान इक़बाल), मुफ्फकिर-ए-पाकिस्तान (पाकिस्तान का विचारक), शायर-ए-मशरीक़ (पूरब का शायर) और हकीम-उल-उम्मत (उम्मा का विद्वान) भी कहा जाता है।
विभाजन का विचार
संपादित करें१९३८ में जिन्नाह को लेकर भाषण का अंश "केवल एक ही रास्ता है। मुसलमानों को जिन्ना के हाथों को मजबूत करना चाहिए। उन्हें मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। भारत की आज़ादी का प्रश्न, जैसा कि अब हल किया जा रहा है, हिंदुओं और अंग्रेजी दोनों के खिलाफ हमारे संयुक्त मोर्चे द्वारा काउंटर किया जा सकता है। इसके बिना, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारी मांग सांप्रदायिक है। यह मिथ्या प्रचार है। ये मांगें हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा से संबंधित हैं .... संयुक्त मोर्चा मुस्लिम लीग के नेतृत्व में गठित किया जा सकता है। और मुस्लिम लीग केवल जिन्ना के कारण सफल हो सकता है। अब जिन्ना ही मुसलमानों की अगुआई करने में सक्षम है।- मुहम्मद इकबाल, १९३८ "[7]
जिन्ना के साथ
संपादित करेंपाकिस्तान बनाने में अग्रणी होने के संबंध में जिन्ना पर इकबाल का प्रभाव बेहद "महत्वपूर्ण", "शक्तिशाली" और यहां तक कि "निर्विवाद" के रूप में वर्णित किया गया है। इकबाल ने जिन्ना को लंदन में अपने आत्म निर्वासन को समाप्त करने और भारत की राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था [8]।अकबर एस अहमद के अनुसार, अंतिम वर्षों में ,१९३८ में उनकी मृत्यु से पहले, इकबाल धीरे-धीरे जिन्ना को अपने विचार अनुसार परिवर्तित करने में सफल रहे, जिन्होंने अंततः इकबाल को उनके "मार्गदर्शक " के रूप में स्वीकार कर लिया। अहमद के अनुसार इकबाल के पत्रों में उनकी टिप्पणियों में, जिन्ना ने इकबाल के इस विचार से एकजुटता व्यक्त की: कि भारतीय मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है।[9]
खुदी का सिद्धांत
संपादित करेंइक़बाल का खुदी का सिद्धांत कहता है की व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए। मनुष्य को नैतिकता और धार्मिक आदर्श जीवन को अपनाना चाहिए,जो सर्वोपरि है जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, नई नई इच्छाएं उसके अंदर सृजित होनी चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
ग्रन्थसूची
संपादित करें- उर्दू में किताबें (गद्य)
- इल्म उल इकतिसाद (1903) [10]
- अंग्रेजी में किताबें प्रस्तावित करें
- फारस में मेटाफिजिक्स का विकास (1908) [11][10]
- इस्लाम में धार्मिक विचारों का पुनर्निर्माण (1930) [11][10]
- फारसी में कविता किताबें
- असरार-ए-खुदी (1915) [10]
- रुमूज़-ए-बेखुदी (1917) [10]
- पयाम-ए-मशरिक़ (1923) [10]
- ज़बूर-ए-अजम (1927) [10]
- जावीद नामा (1932) [10]
- पास चेह बेद कार्ड एआई अकवाम-ए-शर्क (1936) [10]
- अर्मागन-ए-हिजाज़ (1938) [11][10][12] (फारसी और उर्दू में)
- उर्दू में कविता किताबें
इन्हें भी देखें
संपादित करें- सारे जहाँ से अच्छा
- पाकिस्तान आंदोलन
- अल्लामा इकबाल : सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है : https://www.naitahreek.com/2023/08/Allama-Iqbal-sarfaroshi-ki-tamanna-ab-hamare-dil-me-hai.html
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 29 अप्रैल 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2011.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अप्रैल 2018.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अप्रैल 2018.
- ↑ "इकबाल की कलम बनी आवाज, सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां...- News18 Hindi". News18 इंडिया. १७ जुलाई २०१७. मूल से 26 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २६ अप्रैल २०१८.
- ↑ "जन्म-दिन विशेष: देश का "क़ौमी तराना" लिखने वाले अल्लामा इक़बाल थे आधुनिक युग के महान शाइर". The Siasat Daily. ९ नवम्बर २०१६. मूल से 26 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २६ अप्रैल २०१८.
- ↑ Siṃha, P. (2017). Swatantrata Sangharsh Aur Bharat Kee Sanrachana(1883-1984 Ke 75 Bhashnon Mein) (इंडोनेशियाई में). Vāṇī Prakāśana. पृ॰ 15. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-5229-664-4. अभिगमन तिथि २६ अप्रैल २०१८.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 जून 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 मई 2018.
- ↑ https://books.google.com/books?id=jgSOAAAAMAAJ&q=%22it+was+Iqbal+who+encouraged+Jinnah+to+return+to+India.%22&dq=%22it+was+Iqbal+who+encouraged+Jinnah+to+return+to+India.%22&hl=en&sa=X&redir_esc=y
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 3 मई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 मई 2018.
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>का गलत प्रयोग;allamaiqbal.comनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ अ आ इ "Welcome to Allama Iqbal Site". मूल से 21 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 मई 2018.
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>का गलत प्रयोग;brightpk.comनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें| Muhammad Iqbal से संबंधित मीडिया विकिमीडिया कॉमंस पर उपलब्ध है। |
| विकिसूक्ति पर मुहम्मद इक़बाल से सम्बन्धित उद्धरण हैं। |
- Iqbal Cyber Library
- The collection of Urdu poems: Columbia University
- Encyclopedia Britannica.
- Allama Iqbal Urdu Poetry Collection
| यह जीवनचरित लेख एक आधार है। जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने में विकिपीडिया की मदद करें। |